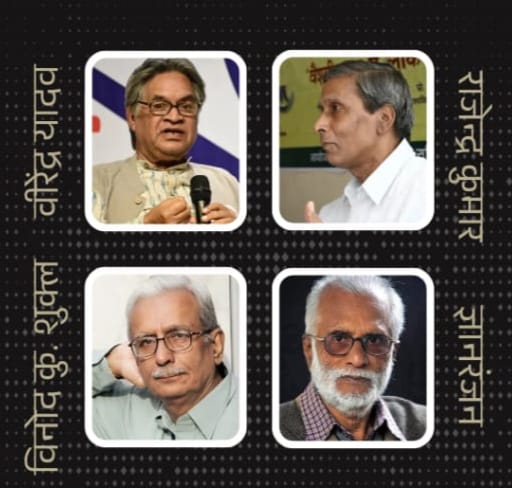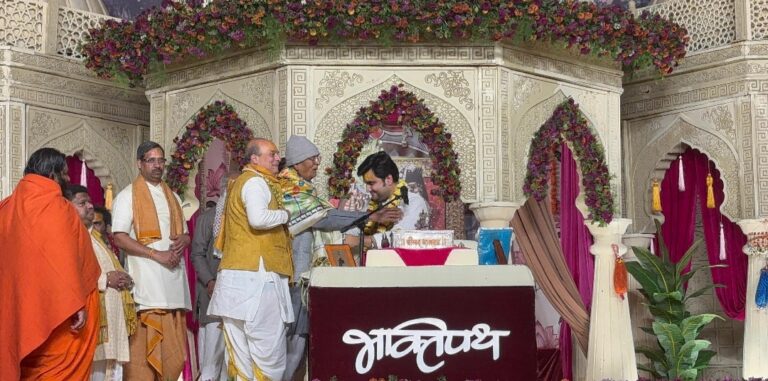राधाष्टमी पर विशेष
डॉ. धर्मराज (प्रोफेसर, श्री बाबूलाल पीजी कॉलेज, गोवर्धन, मथुरा)
समकालीन समाज एक विचित्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। विज्ञान, तकनीक और भौतिक प्रगति ने जहाँ मनुष्य को असीम सुविधाओं से सम्पन्न किया है, वहीं मानवीय भावनाओं का सूक्ष्मतम आयाम ‘प्रेम’ अपने मौलिक स्वरूप से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है। वह प्रेम, जो आत्मा की गहनतम अनुभूति और जीवन की परम अनिवार्यता है, आज आकर्षण, वासना और स्वार्थ की परिधि में सिमट रहा है। बाज़ारवाद और सोशल मीडिया के उपभोक्तावादी प्रभाव ने प्रेम को भी वस्तु बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधों का आधार विश्वास और समर्पण न होकर दिखावे और अधिकार तक सीमित हो गया है, यही कारण है कि छल, अविश्वास और अपराध का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ रहा है। ऐसे समय में स्मरण होता है राधा–कृष्ण के उस दिव्य और शाश्वत प्रेम का, जो लौकिक बन्धनों से परे अद्वैत की अनुभूति कराता है, जहाँ न छल है, न कल, न समय का बन्धन, वहाँ तो केवल और केवल प्रेम है।
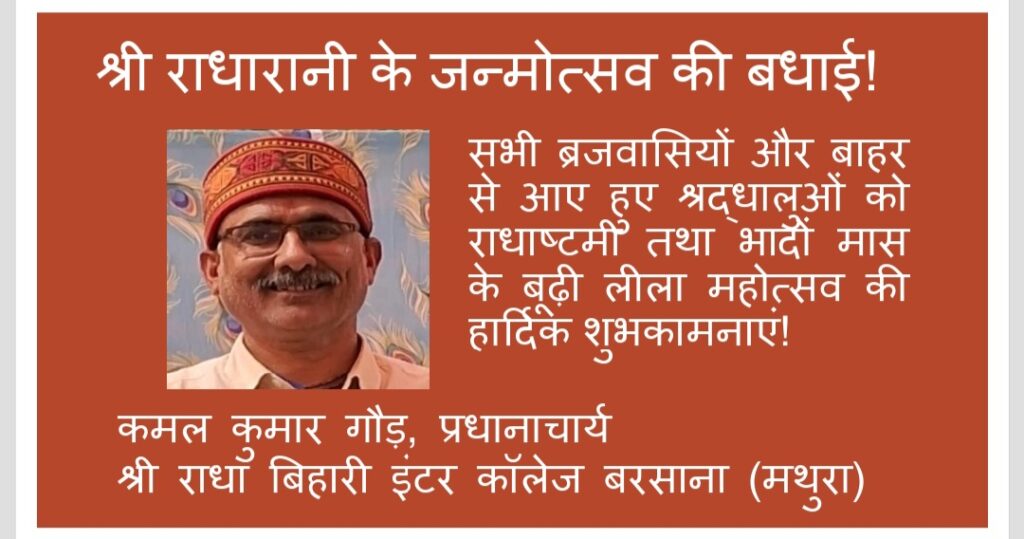
राधा–कृष्ण का प्रेम लौकिक सम्बन्ध ही नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसमें अधिकार का नहीं, अपितु समर्पण का भाव है; वासना का नहीं, अपितु आत्मिक अनुराग के स्वर हैं। जयदेव ने गीतगोविन्द में इस प्रेम को आत्मा की साधना के रूप में रूपायित करते हुए प्रार्थना की, “स्मरगरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं, देहि पदपल्लवमुदारम्।” यहाँ प्रेम वासनाजन्य नहीं, बल्कि उपासना और आत्मविसर्जन का माध्यम है।
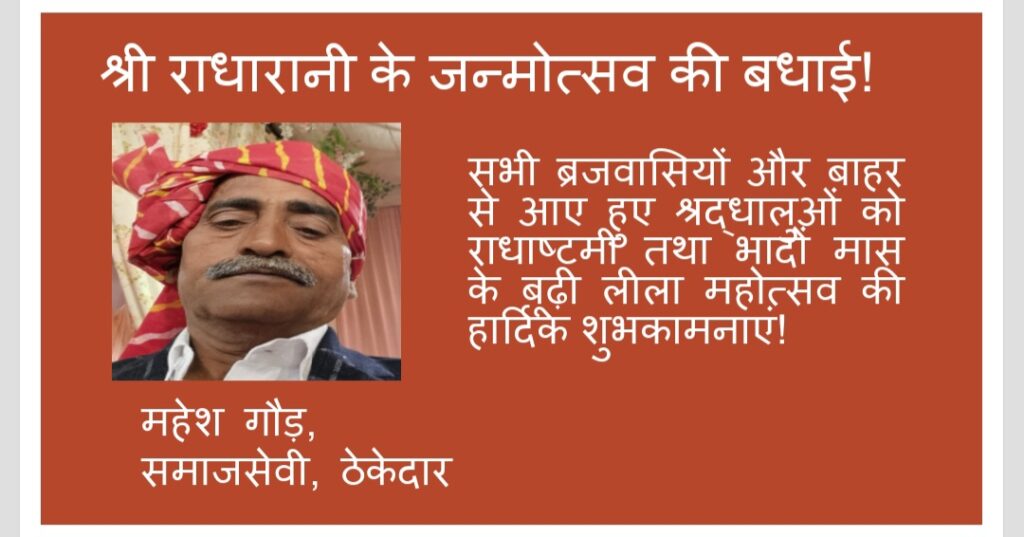
सूरदास ने अपने पदों में राधा–कृष्ण के प्रेम को सहजता और आत्मीयता की चरम परिणति के रूप में चित्रित किया है, उनका बालकृष्ण का चित्रण—“मैया! मोहे दाऊ बहुत खिझायौ…” केवल बाललीला का विनोद न होकर उस निष्कपट आत्मीयता का उद्घोष है, जहाँ प्रेम छलरहित और सच्चा है। रहीम प्रेम को धागे से जोड़ते हुए आगाह करते हैं कि विश्वास के बिना प्रेम क्षणभंगुर है, “रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय।” रसखान का कृष्ण–प्रेम तो इस दिव्य भावधारा का अनुपम उदाहरण है। एक मुसलमान कवि होकर भी उन्होंने गोकुल–वृन्दावन को अपना स्वर्ग स्वीकार किया—“मानुष हौं तो वही रसखान, बसौं मिलि गोकुल गाँव के ग्वालन।” उनके लिए कृष्ण कोई सांस्कृतिक प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि प्रेम के शाश्वत केन्द्र हैं।
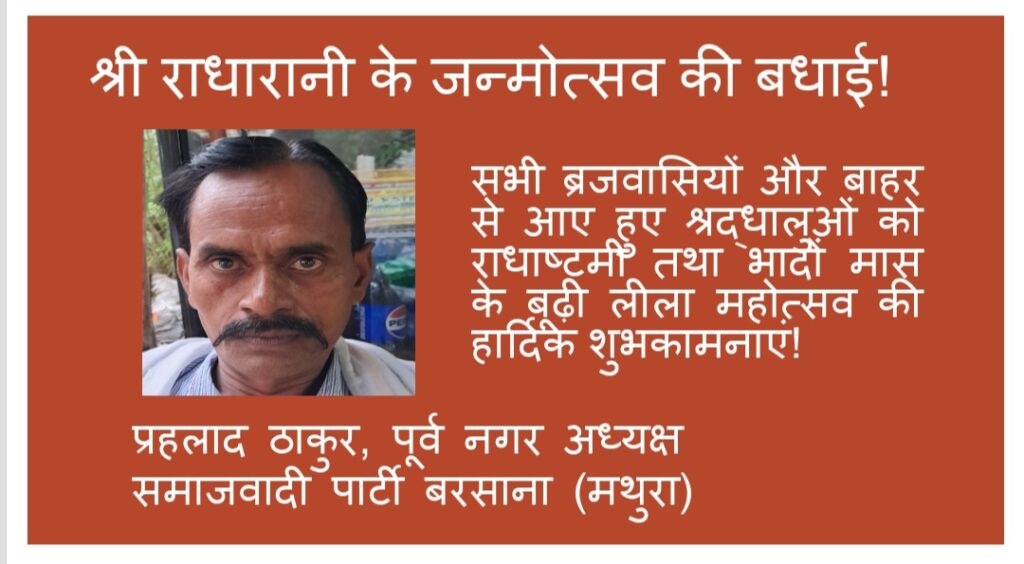
इसी काव्यधारा में घनानन्द का नाम भी अमर है। उनका विरह–रसपूर्ण पद, “अति सूधो सनेह को मारग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं।” जो प्रेम की धरा पर अद्वितीय आदर्श को स्थापित करता है। घनानन्द ने प्रेम को लौकिक आकर्षण नहीं, बल्कि साधना का दुर्गम मार्ग माना, जहाँ द्वैत और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। इसी प्रकार मीरा का कृष्ण–प्रेम भक्ति और अनुरक्ति का चरम उदाहरण है, “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोय।” मीरा ने अपने जीवन को ही कृष्ण–समर्पण का माध्यम बना दिया, यह प्रतिपादित करते हुए कि वास्तविक प्रेम में कोई विकल्प शेष नहीं होता।
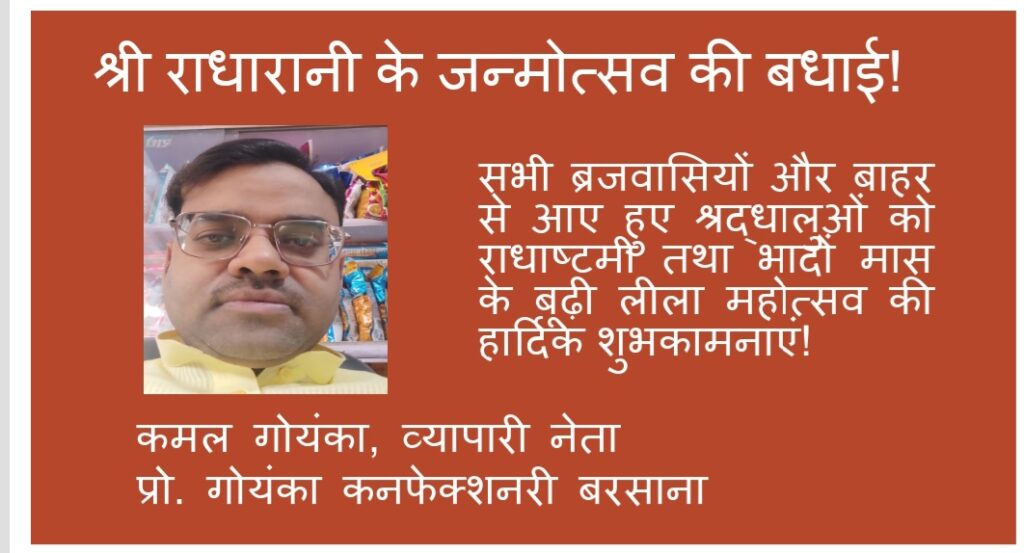
भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में राधा–कृष्ण का प्रेम अनगिनत रूपों में परिभाषित व व्याख्यायित हुआ है। जयदेव की रसधारा, सूर का विरह, रहीम की नसीहत, रसखान का समर्पण, मीरा की भक्ति और घनानन्द की प्रेमदृष्टि, ये सब मिलकर प्रेम के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जिसमें पवित्रता, आत्मीयता और समर्पण ही प्रधान है।
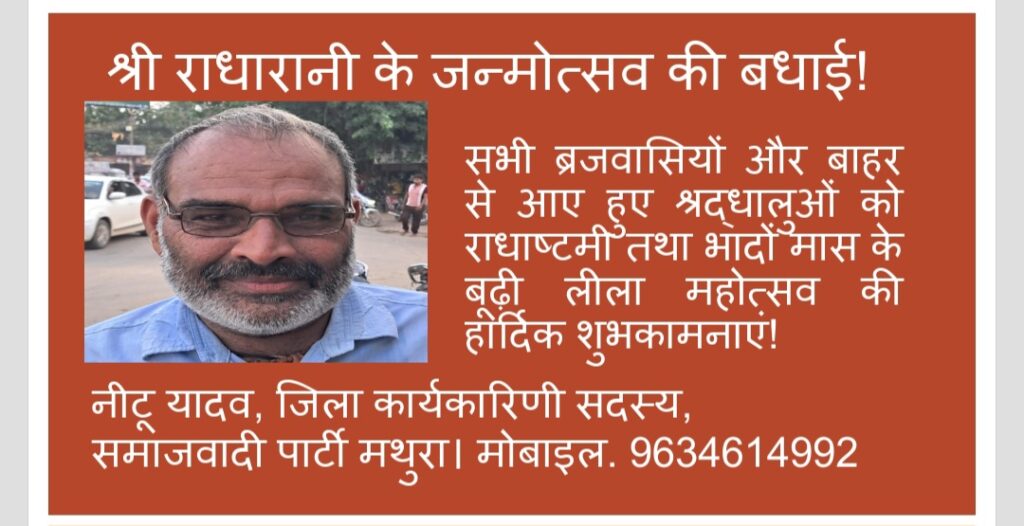
इसके विपरीत, आधुनिक समय में प्रेम का जो विकृत रूप हमारे सम्मुख है, वह समाज को प्रतिदिन खोखला कर रहा है। जब प्रेम अधिकार, वासना और स्वार्थ की जकड़न में कैद हो जाए, तब वह विनाशकारी सिद्ध होता है; किन्तु जब उसकी बुनियाद राधा–कृष्ण का आदर्श हो, तब वही प्रेम जीवन को सौन्दर्य और समाज को नैतिक आधार प्रदान करता है।

आज की युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि प्रेम को केवल क्षणिक आकर्षण या उपभोग का साधन न मानकर उसे आत्मिक साधना के रूप में ग्रहण करे। यदि प्रेम में राधा–कृष्ण जैसी दिव्यता और निस्वार्थता का अंश होगा, तभी वह जीवन और समाज दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकेगा; अन्यथा विकृत होता प्रेम केवल अस्थिरता और पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

अतः जब प्रेम अपने मौलिक स्वरूप से विचलित हो चुका हो, तब राधा–कृष्ण का दिव्य प्रेम हमारे लिए शाश्वत प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत एवं आधार है। यह हमें स्मरण कराता है कि प्रेम का आदर्श पाने में नहीं, अपितु देने में है; अधिकार में नहीं, बल्कि समर्पण में है; क्षणभंगुरता में नहीं, बल्कि शाश्वतता में है। यही वह चेतना है, जिसे भारतीय संस्कृति ने युगों–युगों से संजोया है और जिसे आत्मसात् करके ही हम प्रेम के विकृत होते स्वरूप को परिष्कार कर सकते हैं।
डॉ धर्मराज (प्रोफेसर, श्री बाबूलाल पीजी कॉलेज, गोवर्धन, मथुरा)